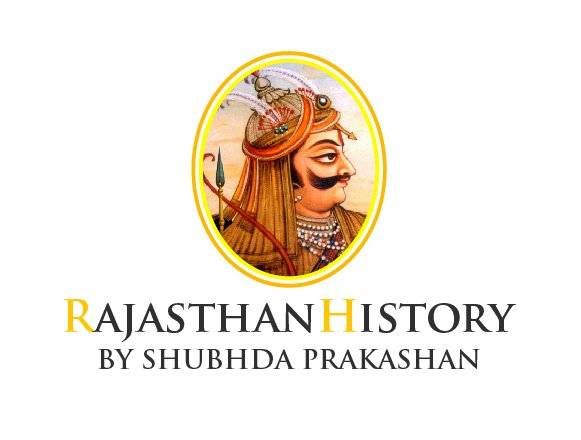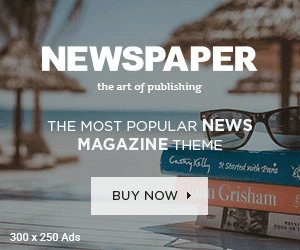राजस्थान का राजनीतिक एकीकरण, जटिल एवं दीर्घकालीन प्रक्रिया थी जिसके कारण राजस्थान का वातावरण हलचलों से भरा हुआ तथा उत्तेजनापूर्ण बना हुआ था किंतु राजस्थान का प्रशासनिक एकीकरण उससे भी अधिक जटिल एवं कठिन था जिसके लिए असीम धैर्य और कठोर परिश्रम की आवश्यकता थी।
लोकप्रिय सरकार का गठन
30 मार्च 1949 को सरदार पटेल द्वारा राजस्थान का विधिवत् उद्घाटन कर दिए जाने के बाद 4 अप्रेल 1949 को हीरालाल शास्त्री ने राजस्थान का कार्यभार संभाला। 7 अप्रेल 1949 को मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल का गठन किया। सिद्धराज ढड्ढा (जयपुर), प्रेमनारायण माथुर और भूरेलाल बयां (उदयपुर), फूलचंद बाफना, नरसिंह कच्छवाहा और रावराजा हनुवंतसिंह (जोधपुर), रघुवरदयाल गोयल (बीकानेर) और वेदपाल त्यागी (कोटा) को मंत्रिमण्डल में लिया गया।
मंत्रिमण्डल के गठन वाले दिन ही अर्थात् 7 अप्रेल 1949 को राजस्थान सरकार ने जोधपुर, जयपुर, बीकानेर तथा जैसलमेर राज्यों का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। इसके साथ ही राजस्थान का प्रशासनिक एकीकरण आरम्भ हो गया।
समस्याएं दर समस्याएं
सैंकड़ों साल से अस्तित्व में बनी हुई 19 देशी रियासतों एवं 3 बड़े ठिकानों को एक ही प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत लाना एक बड़ी चुनौती थी। इन रियासतों के आकार, जनसंख्या, आर्थिक स्थिति, प्रशासनिक एवं न्यायिक प्रशासन, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रीति-रिवाज तथा बोली जाने वाली भाषाओं में काफी अंतर था। अधिकांश राज्यों का प्रशासन अब भी मध्यकालीन परम्पराओं और पुरातन पद्धतियों से चलता आ रहा था।
जयुपर, जोधपुर, बीकानेर एवं उदयपुर आदि कुछ राज्यों में ही अंग्रेजी प्रांतों जैसी आधुनिक सरकारों की स्थापना हो पाई थी। इन राज्यों में मंत्री परिषदों का गठन हो गया था जिनमें लोकप्रिय मंत्री कार्य कर रहे थे।
कुछेक राज्यों में लोकसेवा आयोग के माध्यम से नियुक्तियां होने लगी थीं तथा सुस्पष्ट नियमों एवं योग्यता के आधार पर पदोन्नतियां दी जाती थीं। जबकि बहुत से राज्यों में अब भी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग नहीं किया गया था। कुछ राज्यों में भ्रष्टाचार से निबटने के लिये भ्रष्टचार निरोधक विभाग बन चुके थे और राजकीय खातों के अंकेक्षण की भी व्यवस्था थी। जबकि अधिकांश राज्यों में ऐसा कुछ नहीं था।
राजस्थान के गठन के साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को स्थायित्व देने तथा समुचित कोष जुटाने के प्रयासों की आवश्यकता थी। राज्य के प्रशासनिक ढांचे को विकसित करने के लिये नियम एवं कानून बनाने का काम आरम्भ किया जाना था। नयी सेवाओं की स्थापना करना, लेखा नियम बनाना तथा विभिन्न राज्यों की सेवाओं का एकीकरण करना एक दुसाध्य कार्य था। इस प्रकार राजस्थान का प्रशासनिक एकीकरण एक जटिल प्रक्रिया थी।
राजधानी के बार-बार बदले जाने से उत्पन्न समस्या
प्रथम राजस्थान संघ की राजधानी कोटा में रखी गयी थी। इसके बाद जब द्वितीय राजस्थान अर्थात् संयुक्त राजस्थान बना तो उसकी राजधानी उदयपुर में रखी गयी। तृतीय राजस्थान अर्थात वृहत् राजस्थान की राजधानी जयपुर में रखी गयी। वृहत् राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय होने पर मत्स्य संघ की राजधानी जयपुर लायी गयी। राजधानी के बार-बार बदले से हर बार सरकारी तंत्र तथा अभिलेख एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के कारण राजस्थान का प्रशासनिक एकीकरण एक लम्बी प्रक्रिया से गुजरा किंतु इस समस्या को धैर्यपूर्वक सुलझा लिया गया तथा जयपुर के राजधानी बनने के बाद यह समस्या स्वतः समाप्त हो गयी।
रियासती कस्टम सीमाओं की समाप्ति
मंत्रिमंडल के गठन वाले दिन अर्थात् 7 अप्रेल 1949 को राज्य सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर अंतर रियासती कस्टम सीमाओं को समाप्त कर दिया। इस प्रकार अब तक चली आ रही रियासत कालीन व्यवस्थाएं 7 अप्रेल 1949 से पूर्णतः समाप्त हो गयीं। राजस्थान का प्रशासनिक एकीकरण धरातल पर आने लगा।
पाकिस्तान से लगी सीमा की सुरक्षा
भारत की आजादी के साथ ही भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा अस्तित्व में आई। वृहत् राजस्थान में सम्मिलित बीकानेर, जैसलमेर तथा जोधपुर रियासतें इस सीमा पर स्थित थीं। राजस्थान बनने के बाद इस सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार पर आ गयी। राजस्थान के वित्तीय संसाधनों में यह संभव नहीं था कि वह इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा के लिए सेना का गठन कर सकती। अतः यह कार्य केन्द्र सरकार को दिया गया।
संघीय इकाई का प्रशासन केन्द्र के हाथों में
स्वतंत्र भारत में एकीकृत होने वाली संघीय इकाइयां (अर्थात् राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि) भारत सरकार की पहल पर बन रही थीं किंतु भारत सरकार का इन संघों पर कोई संवैधानिक नियंत्रण नहीं था। अप्रिय घटित होने पर भारत सरकार कानूनी रूप से कुछ नहीं कर सकती थी।
अब तक जो नियंत्रण बन पाया था वह सरदार पटेल के व्यक्तित्व द्वारा बनाया गया था। इन संघों में मिलने वाले राज्यों के शासकों को उस प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता था जिस प्रकार की कठिनाईयां प्रांतीय सरकारों के सामने आ रही थीं। इन कठिनाईयों से निबटने के लिये प्रांतीय सरकारों के पास किसी तरह के संवैधानिक उपकरण नहीं थे। राजनैतिक संगठनों के पास भी प्रशासन चलाने के लिये अनुभवी एवं योग्य नेता नहीं थे। राजस्थान का प्रशासनिक एकीकरण ही इस समस्या को सुलझा सकता था।
राज्यों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निष्ठाएं रातों-रात नहीं बदली जा सकती थीं। अनुभवहीन नेताओं तथा राजनैतिक अधिकारों से अनभिज्ञ जनता के भरोसे प्रशासन नहीं छोड़ा जा सकता था। विशेषज्ञ मार्गदर्शन दिया जाना आवश्यक था। यह भी देखना था कि राज्यों के एकीकरण एवं उनके प्रजातंत्रीकरण की प्रक्रिया पूर्ण गति एवं दक्षता से पूरी हो।
रियासती विभाग के सचिव वी. पी. मेनन ने सुझाव दिया कि जब तक राजस्थान की स्थानीय विधानसभा अपने लिये संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक राजप्रमुख तथा मंत्रिमण्डल भारत सरकार के सामान्य नियंत्रण में रहें तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों की पालना करें।
यह व्यवस्था राजस्थान का प्रशासनिक एकीकरण करने में बहुत सहायक सिद्ध हो सकती थी। इस कारण प्रशासनिक अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को तुरंत मान लिया किंतु लोकप्रिय नेताओं ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। लम्बे चौड़े बहस-मुसाहबे के बाद नेताओं ने भी इस प्रस्ताव को मान लिया। बाद में राजस्थान प्रसंविदा का यह प्रावधान अन्य राज्यों के लिये भी कर दिया गया।
राजस्थान प्रसंविदा में अनिवार्य रूप से यह प्रावधान किया गया था कि राजप्रमुख एक नवीन विलयपत्र अमल में लायेंगे जिसके अनुसार भारत की संविधानसभा द्वारा कर एवं शुल्क को छोड़कर, संघीय एवं राज्य की विधानसभा के विधान की समवर्ती सूची में शामिल किये जाने वाले समस्त विषयों को स्वीकार किया जाना आवश्यक था।
रियासती सेनाओं का राष्ट्रीयकरण
ई.1939 में इण्डियन स्टेट्स फोर्सेज स्कीम के तहत रियासती सेनाओं में तीन प्रकार की इकाइयां रखी गयीं थीं- फील्ड सर्विस यूनिट्स, जनरल सर्विस यूनिट्स तथा स्टेट सर्विस यूनिट्स। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश के 44 राज्यों की सेनाएं इण्डियन स्टेट्स फोर्सेज स्कीम के तहत थीं जिनमें 75,311 अधिकारी थे। शेष राज्यों में इस योजना से बाहर की सेनाएं थीं जिनमें अधिकतर पुलिस तथा अंलकरण इकाइयां थीं।
आजादी के बाद कश्मीर अभियान तथा अन्य कठिन परिस्थितियों में भारत सरकार को जब सेनाओं की आवश्यकता हुई तो भारतीय सेनाओं की कई टुकड़ियां नियत स्थानों पर नहीं पहुँचीं। इस पर भारत सरकार ने राज्यों से अनुरोध किया कि वे अपनी सेनाएं भेजें। अगस्त 1947 के प्रविष्ठ संलेख में राज्य की सुरक्षा का विषय केंद्र सरकार को दिया गया था। इसलिये राज्यों की सेनाओं को भारत सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया।
जो सेना जहाँ नियत थी उसे वहीं रखा गया, उनके कार्य की शर्तों तथा परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके बाद योग्य सैनिकों को सेना में ग्रहण करने का कार्य शनैः-शनैः किया गया। जो सैनिक भारतीय सेना के मानकों के अनुरूप नहीं पाये गये, उन्हें समुचित रियायत देकर सेना से मुक्त कर दिया गया।
राज्यों की सेनाओं पर नियंत्रण स्थापित करने के लिये कई उपाय किये गये-
(1.) इन बलों का नियंत्रण राजप्रमुख के अधीन भारतीय सेना के किसी अधिकारी द्वारा किया जाये।
(2.) इन बलों की संख्या तथा संगठन भारतीय प्रतिरक्षा के संदर्भ में निश्चित किया जाये।
(3.) इन बलों का पुनर्गठन भारतीय सेना के मानकों के अनुसार किया जाये।
(4.) अधिकारियों का चयन भारतीय सेना की चयन प्रक्रिया के अनुसार किया जाये। उनकी पदोन्नति आदि भी उसी तरह नियंत्रित की जाये।
(5.) भारतीय सेनाओं तथा इन बलों के अधिकारियों की निश्चित संख्या में अदला-बदली की जाये।
राज्यों का वित्तीय एकीकरण किये जाने के बाद इन बलों का व्यय केन्द्र सरकार द्वारा उठाया जाने लगा तथा 1 अप्रेल 1951 को ये सेनाएं पूरी तरह भारतीय सेना का हिस्सा बन गयीं।
राजस्थान के राजप्रमुख महाराजा मानसिंह को रियासती सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। राजप्रमुख के नीचे बीकानेर रियासत के प्रधान सेनापति जनरल जयदेवसिंह को रखा गया। राजपूताने की रियासतों की सेनाओं के एकीकरण के मामले में काफी असंतोष उभर कर सामने आया। कई लोगों को शारीरिक योग्यता के कारण नौकरी से छुट्टी दे दी गयी।
ट्रेकोमा (आंखों में दाने पड़ जाना) को सेना के लिये अयोग्यता का कारण माना गया और बहुत से सैनिकों को इसके आधार पर हटाया गया। वरिष्ठता निश्चित करने या भारतीय सेना में पदोन्नति के लिये रियासती सेना के अधिकारियों की नौकरी की अवधि घटा दी गई।
यह नियम बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर जैसी रियासतों पर भी लागू हुआ जबकि इन रियासतों में प्रथम श्रेणी की सेना थी। भारतीय सेना में रियासती सेनाओं के जो अधिकारी लिये गये उनमें से बहुतों की बाद में पदावनति कर दी गयी तथा उन्हंे आर्थिक हानि उठानी पड़ी। राजस्थान की सेनाओं के भारतीय सेना में मिलने से राजप्रमुख भी राजस्थान की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति नहीं रहा। विभिन्न रियासतों की सेनाओं का एकीकरण किए बिना राजस्थान का प्रशासनिक एकीकरण किया जाना संभव नहीं था।
सरकार पर आई. सी. एस. अधिकारियों का नियंत्रण
राजस्थान का प्रशासनिक एकीकरण करने के लिये भारत सरकार द्वारा तीन अनुभवी आई. सी. एस. अधिकारी केन्द्र से भेजे गये। इन्हें राजस्थान सरकार में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। इन आई. सी. एस. अधिकारियों को अधिकार दिया गया कि वे मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री एवं मंत्री के किसी भी निर्णय पर वीटो कर सकते हैं।
राज्य अधिकारियों का एकीकरण
विभिन्न राज्यों के अधिकारियों की सेवाओं का राजस्थान सरकार द्वारा एकीकरण किया गया। विभिन्न राज्यों में अधिकारियों के पदनाम तथा उनके वेतनमान में अंतर के कारण भारी विसंगतियां उत्पन्न हो गयीं। कुछ बड़े राज्यों में राजस्थान बनने से पहले कर्मचारियों एवं अफसरों के वेतन मनचाही रीति से बढ़ा दिये गये।
जोधपुर राज्य के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी गणेशदत्त छंगाणी, जो उन दिनों राज्य के पैट्रोल राशनिंग ऑथोर्टी तथा जोधपुर राज्य के लोकसेवा आयोग के सचिव भी थे, ने अन्य राज्यों द्वारा कर्मचारियों के वेतनमानों में की गई वृद्धि का तुलनात्मक चार्ट बनाकर जोधपुर राज्य के मुख्यमंत्री जयनाराण व्यास के सम्मुख प्रस्तुत किया किंतु व्यास ऐसा नहीं कर सके जिससे जोधपुर राज्य के कर्मचारी अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ गये।
जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री ने भी ऐसा नहीं किया इससे जयपुर के अफसर भी घाटे में रह गये। राज्याधिकारियों का एकीकरण काफी उलझन भरा था। एकीकरण की प्रक्रिया में कुछ ऐसी शिकायतें आईं कि कुछ राज्यों के तहसीलदार, राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आ गये और कुछ रियासतों के विभागाध्यक्ष तहसीलदार बना दिये गये।
कुछ लिपिकों को सहायक सचिव एवं सहायक सचिवों को लिपिक बना दिया गया। सचिवालय में सचिवों, उपसचिवों एवं विभागाध्यक्षों के प्रायः सभी स्थानों पर केंद्र अथवा अन्य राज्यों के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लाकर नियुक्त कर दिया गया। फलस्वरूप विभिन्न रियासतों से आये हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों में भयंकर असंतोष फैल गया। कुछ समय के लिए सभी स्तरों पर राज्यकार्य ठप्प सा हो गया इस प्रकार राजस्थान का प्रशासनिक एकीकरण समस्त पूर्व रियासतों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तर्क संगत न्याय नहीं दे सका।
वित्तीय एकीकरण
राज्यों के वित्तीय एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा वित्तीय आंकड़ों की अनुपलब्धता थी। भारत की संविधानसभा द्वारा राज्यों के वित्तीय एकीकरण के उपाय सुझाने के लिये नलिनी रंजन सरकार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसने दिसम्बर 1947 में सुझाव दिया कि समस्त राज्यों में संपूर्ण देश के समान कर-व्यवस्था लागू होनी चाहिये। यह व्यवस्था 15 वर्ष के लिये लागू की जानी चाहिये।
समस्त राज्यों को निर्देशित किया गया कि वे राज्य के बजट का निर्माण आवश्यक रूप से करें तथा खातों व लेखों की अंकेक्षण व्यवस्था करें। 22 अक्टूबर 1948 को वी. टी. कृष्णामाचारी की अध्यक्षता में ‘इण्डियन स्टेट्स फाइनेंसेज इंक्वायरी कमेटी’ का गठन किया गया। विभिन्न राज्यों तथा संघराज्यों ने इस समिति का विरोध किया क्योंकि राज्य तथा राज्यसंघ वित्तीय मामालों में केंद्र का हस्तक्षेप नहीं चाहते थे।
1 अप्रेल 1950 को राज्य का वित्तीय एकीकरण हुआ। इसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा रेलवे, सेना और ऑडिट विभाग तथा उससे सम्बन्धित स्थावर और जंगम संपत्ति भारत सरकार को बिना किसी मुआवजे के सौंप दी गयी। राज्य पर बाह्य आक्रमणों से निबटने का उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार पर चला गया। वित्तीय एकीककरण किए बिना राजस्थान का प्रशासनिक एकीकरण संभव नहीं था।
कानून व्यवस्था की समस्या
राजस्थान के अस्तित्व में आने के समय अधिकांश राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई थी तथा प्रशासन अत्यंत बदतर अवस्था में था। कानून सतही तथा अपर्याप्त थे। प्रशासनिक प्रक्रियाएं सुस्पष्ट नहीं थीं। बड़ी सीमा तक प्रशासन व्यक्तिगत प्रकृति का था तथा राजा और उसके सलाहकारों की मर्जी से चलता था।
नवनिर्मित राजस्थान में इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था को एक स्तर पर लाना सबसे बड़ी चुनौती थी। सबसे पहला कार्य डकैतों और लुटेरों पर काबू पाकर कानून की पुनर्स्थापना करने का था जो कि गाँवों और दूर दराज के क्षेत्रों में आतंक मचाये हुए थे। यह कार्य बहुत शीघ्रता और अत्यंत दक्षता से किया गया।
जागीरदारी व्यवस्था की समाप्ति
राजस्थान का प्रशासनिक एकीकरण यदि किसी बिंदु पर आकर उपझ सकता था तो वह थी परम्परागत रूप से चली आ रही जागीरदारी व्यवस्था। राजस्थान की रियासतों में राजस्व संग्रहण की दृष्टि से दो प्रकार की भूमि थी, खालसा भूमि तथा जागीरी भूमि। खालसा भूमि के अंतर्गत 50,126 वर्गमील तथा जागीरी भूमि के अंतर्गत 77,110 वर्गमील क्षेत्रफल था। राजस्थान के 16,638 गाँव खालसा के अंतर्गत तथा 16,780 गाँव जागीरों के अंतर्गत आते थे।
जागीरदारों को परम्परागत रूप से अपनी जागीर में मालगुजारी वसूलने का अधिकार था किंतु राजस्थान संघ के बनने से चूंकि रियासतें ही नहीं रह गयीं थीं इसलिये जागीरी प्रथा नितांत अप्रासंगिक हो गयी थी। विभिन्न राज्यों के प्रजामण्डलों एवं प्रजापरिषदों जैसी लोकप्रिय संस्थाओं ने जागीरों को समाप्त करने की मांग की किंतु जागीरदार अपने अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं थे। कई जगहों पर प्रजामण्डलों के कार्यकर्ताओं एवं जागीरदारों के आदमियों में झड़पें हुईं।
25 जनवरी 1949 को सरदार पटेल जोधपुर आए तथा उन्होंने वहाँ आयोजित एक आमसभा में कहा-
‘जागीरदार बदले हुए समय को पहचानें। जो लोग गलत काम करते हुए पाये जायेंगे उनसे दूसरी तरह का व्यवहार किया जायेगा। जागीरदारों को समझना चाहिये कि गलत क्या है!
उन्हें यह भी समझना चाहिये कि आज के युग में बड़े और छोटे का भेद तथा स्वामी और सामान्य आदमी का भेद समाप्त हो गया है तथा यह प्रचलन से बाहर हो गया है। उन्हें उन लोगों के भाग्य से सबक लेना चाहिये जो प्रजातंत्र के साथ नहीं चले या एकीकरण की प्रक्रिया के साथ नहीं चले। हमने एकीकरण की दिशा में जो कुछ भी प्राप्त किया है वह राजाओं की साख और सहयोग से प्राप्त किया है।
कोई भी जागीरदार बलपूर्वक, डकैती से या बदला लेने की विधि से कुछ भी हासिल नहीं कर सकेगा। यह एक परिणामहीन व्यापार है। भारत उपनिवेश शांति तथा सुरक्षा के लिये उत्तरदायी है। सरदार पटेल ने मारवाड़ प्रजापरिषद के नेताओं तथा स्थानीय कांग्रेसी नेताओं को सलाह दी कि वे जागीरदारों का अपमान करने वाली टिप्पणियां न करें। उन्हें जागीरदारों की समस्या को समाप्त करने के लिये समझाइश से काम लेना चाहिये तथा जागीरदारों के हृदय में स्थान बनाना चाहिये।’
भारत सरकार के प्रस्ताव संख्या आर (61)-पी/49 दिनांक 30 अगस्त 1949 को यह प्रस्ताव किया गया कि राजस्थान तथा मध्यभारत की जागीरों के सम्बन्ध में एक समिति बनायी जाये जो इन जागीरों का भविष्य तय करने के लिये अपनी रिपोर्ट प्रदान करे।
इस क्रम में सी. एस. वेंकटाचार की अध्यक्षता में एक समिति बनायी गयी जिसमें राजस्थान से गोकुलभाई भट्ट एवं सीताराम जाजू को तथा मध्य भारत से ब्रजचंद शर्मा एवं वी. विश्वनाथन को लिया गया। इस समिति ने 18 दिसम्बर 1949 को अपनी रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया कि जागीरदारी प्रथा समाप्त होनी चाहिये तथा राजस्व संग्रहण का कार्य सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होना चाहिये।
जागीरदारी अधिकार सम्पत्ति के अधिकार नहीं हैं अतः जागीरदारों को कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जानी चाहिये। जिन जागीरदारों के नियंत्रण में पूरा गाँव है, उन्हें पुनर्वास सहायता दी जानी चाहिये। जागीर के लिये वार्षिक मूल्य दिया जाना चाहिये।
जागीरदारों, माफीदारों इत्यादि को उनके अधिकार वाली कृषि जोत तथा भूखण्डों की पूर्ण वार्षिक आय अगले 12 वर्षों तक दी जानी चाहिये। काश्तकारों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिये ताकि जागीरदार उनकी भूमि को हड़प न सकें। इस समिति द्वारा सुझाए गए उपायों के आधार पर ही जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। इससे असंतोष तो बना रहा किंतु समय के साथ वह स्वतः समाप्त हो गया।
सुवाणा गोली काण्ड
21 जुलाई 1949 को भीलवाड़ा जिले के सुवाणा गांव में लेवी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने फायरिंग की जिससे 21 से अधिक किसान मारे गये और अनेक घायल हो गये। मुख्यमंत्री ने इस कांड के लिये स्थानीय नेताओं को दोषी ठहराया। न तो मुख्यमंत्री स्वयं और न मंत्रिमण्डल का कोई सदस्य घटना स्थल पर पहुँचा। इससे क्षुब्ध होकर समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने इस काण्ड की तुलना जलियांवाला कांड से की तथा 29 जुलाई 1949 को सुवाणा दिवस मनाने का आह्वान किया।
राजस्थानी कहलाने में होता है गर्व
इस प्रकार संयुक्त राजस्थान संघ, बड़ी तेजी से एकीकरण की प्रक्रिया से गुजरा। 2 मार्च 1952 तक इस राज्यसंघ में लोकप्रिय सरकारें काम करती रहीं। 3 मार्च 1952 को मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल के नेतृत्व में जनता द्वारा चुनी हुई पहली सरकार अस्तित्व में आई और लोकतांत्रिक राजस्थान अस्तित्व में आ गया। राज्य की जनता स्वयं को राजस्थानी कहने और कहलाने में गर्व का अनुभव करती है जो इस बात का द्योतक है कि राजस्थान का प्रशासनिक एकीकरण पूरी तरह से सम्पन्न हो चुका है।
-डॉ. मोहनलाल गुप्ता