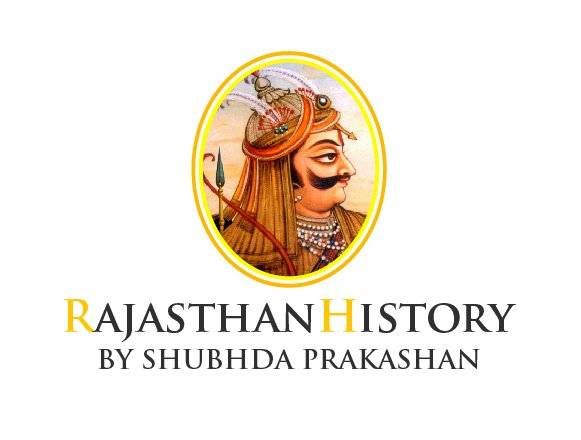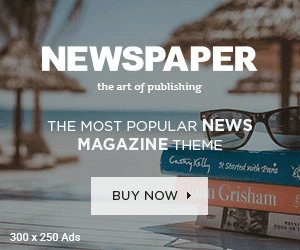परमारों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रायः सभी इतिहासकारों ने उन्हें अग्निवंशीय माना है और सभी ने आबू पर्वत पर वशिष्ठ ऋषि के अग्निकुण्ड को उनके जन्मस्थल के रूप में निर्दिष्ट किया है। परम्परा के आधार पर परमारों को अग्निवंशी कहने में कोई आपत्ति नहीं, परंतु अग्निकुण्ड से किसी पुरुष की उत्पत्ति मानना असंभव है। इसलिए विद्वानों ने परमारों की उत्पत्ति पर इस परम्परा को छोड़कर भिन्न आधारों पर भी विचार किया है। फलतः इस सम्बन्ध में अनेक मत प्रतिपादित हुए है।
कुछ विद्वान परमारों को गुर्जर सिद्ध करने का प्रयास करते हैं तो अन्य उन्हें राष्ट्रकूटों की शाखा मानते हैं। इन मतों की भली प्रकार समीक्षा की जा चुकी है [1] और यह स्पष्ट हो चुका है कि इन सिद्धांतों के पक्ष में दिये जाने वाले तर्क निस्सार हैं। [2] परमार न तो गुर्जर हैं और न राष्ट्रकूट।
परमारों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में आजकल दो धारणाएँ प्रमुख रुप से प्रचलित हैं। पहली धारणा के अनुसार परमार मालव थे और दूसरी धारणा के अनुसार परमार मूलतः ब्राह्मण थे। प्रथम सिद्धांत के प्रवर्तक डा. दिनेशचन्द्र सरकार हैं जिन्होंने अपनी दो पुस्तकों में इस सम्बन्ध में विचार किया है। [3]
दिनेशचन्द्र सरकार के मत में परमारों के पहले अवन्ति का नाम मालवदेश नहीं था। इस स्थान का नाम मालव होने का कारण, सरकार का मत था कि परमार मूलतः मालव थे, अतः इस प्रदेश पर परमारों के अधिकार के साथ ही इस स्थान का नाम भी मालव देश हो गया।
परमार राजा वाक्पति और उसके उत्तराधिकारी ‘खेटक’ के शासक थे, जो कि ह्वेनसांग के वर्णन में आए मो-ला-पो (मालव) क्षेत्र के अन्तर्गत था। धनपाल के ग्रंथ ‘पाइयलच्छी’ में मान्यखेट को लूटने वाले हर्ष सीयक की सेनाओं को मालव कहा गया है। सीयक के पुत्र वाक्पति (मुंज) ने सबसे पहले उज्जयिनी अर्थात् आधुनिक पश्चिमी मालवा के क्षेत्र में लगभग ई.975 में, जबकि उसने अपना धर्मपुरी दानपत्र जारी किया, परमार शक्ति को सबसे पहले स्थापित किया। डा. सरकार के तर्क भ्रान्त धारणाओं पर आधारित हैं। [4]
यह धारणा भी निराधार है कि परमारों के पूर्व अवन्ति का नाम मालवदेश नहीं था। अवन्ति मालवा के अन्तर्गत ही था, यह तथ्य 7वीं शताब्दी के लेखक बाण द्वारा रचित कादम्बरी के वर्णन से स्पष्ट है। प्रसंगवश कुछ पंक्तियों का उल्लेख किया जा सकता है-
‘उज्जैनी को चारों ओर परिवेष्टित कर शिप्रा नदी प्रवाहित हो रही है, उसका जल यौवन-मद से मतवाली मालवदेश की स्त्रियाँ के कुछ कलशों से शोभित हुआ।‘ [5]
‘जिस उज्जैनी में दूर तक फैली हुई ऊंची ध्वजा रुपी भुजा वाली अट्टालिकाएं ऐसी प्रतीत होती हैं मानो वे रात्रि को मालव-सुन्दरियों के मुखकमल कान्ति देखने से लज्जित हुए चन्द्र के कलंक को पवन से कम्पित होकर फहराती हुई वस्त्र की कोरों से मिलाती है।‘ [6]
‘दशकुमारचरित’ में स्पष्ट रूप से अवन्ति को मालव देश लिखा गया है। [7] इस ग्रंथ में मालवदेश के राजा मानसार व मगधराजा राजहंस के युद्ध की कथा है। शक संवत् 705 में रचित कुवलयमाला में अवन्ति को मालवदेश की राजधानी कहा गया है।[8]
वाक्पति और उसके उत्तराधिकारी खेटक पर राज्य करते थे और वाक्पति (द्वितीय) ने उज्जैनी पर सबसे पहले अधिकार किया, ऐसा मानने के लिए भी कोई प्रमाण नहीं है। सभी अभिलेखों में परमारों का मूल अभिजन आबू बताया गया है। उदैपुर (ग्वालियर) प्रशस्ति में वाक्पति प्रथम के लिए लिखा है कि ‘वह अवन्ति की तरुणियों के नेत्र रूपी कमलों के लिए सूर्य समान था।‘ [9]
यह कथन वाक्पति प्रथम का अवन्ति पर अधिकार सिद्ध करता है। किसी भी परमार अभिलेख में उसके द्वारा अवन्ति जीते जाने का उल्लेख नहीं है। यह स्थान तो आरंभ से ही उसके अधिकार में रहा प्रतीत होता है। यहाँ परमारों से आशय उपेन्द्र और उसके वंशजों से है।
पाइयलच्छी नाम माला में लिखा है-
विक्कमकालस्स गए अउणतीसुतरे सहस्सम्मि मालवनरिदधाडीए लूडिए मन्नखेडम्मि ‘
छाया- ‘विक्रमकालस्य गते एकोनत्रिशदुत्तरे सहसे मालव नरेन्द्रधाद्या लुष्टिते मत्रखेडे‘
इस प्रसंग में कहीं भी सेनाओं को मालव नहीं कहा गया है अपितु स्पष्ट रूप से मालव नरेन्द्र शब्द का प्रयोग है। यह शब्द मालवदेश के शासक के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है न कि मालव जन के शासक के अर्थ में। ऊपर यह बताया जा चुका है कि मालव देश में स्थित अवन्ति में परमारों का राज्य था। अतः मालवदेश के शासक को मालव नरेन्द्र कहना अनुचित नहीं है।
इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि डा. सरकार की यह धारणा, कि परमारों की उत्पत्ति मालवों से हुई अथवा परमार मालव थे, उचित नहीं है।
परमारों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में दूसरे मत के प्रवर्तक डा. दशरथ शर्मा हैं। [10] डा. प्रतिपाल भाटिया [11] ने भी इसी प्रकार का मत व्यक्त किया है। परमारों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सबसे प्राचीन उल्लेख मुंज के दरबारी पंडित हलायुध का है। [12] उसने ‘पिंगलसूत्रवृति’ में मुंज के लिए ‘ब्रह्मक्षत्रकुलीन’ शब्द का प्रयोग किया है। इससे स्पष्ट है कि परमार उस समय ब्रह्मक्षात्र कुल के माने जाते थे।
इस आधार पर डा. दशरथ शर्मा ने लिखा है- ‘संभवतः ब्रह्मक्षत्र शब्द से वे जातियां गणित होती थीं जिनमें ब्राह्मणों और क्षत्रियों दोनों के गुण विद्यमान हों। परमार विद्वान थे और वीर भी, अतः ब्रह्मक्षत्र शब्द उनके लिए उपयुक्त था। यह भी संभव है कि परमार आरंभ में ब्राह्मण हों, धर्म को संकट में देखकर शुंग, सातवाहन, कदम्ब, पल्लव आदि ब्राह्मण कुलों की ही भांति उन्होंने भी तलवार संभाली और समय पाकर क्षत्रिय माने जाने लगे।’
डा. प्रतिपाल भाटिया ने भी इन तथ्यों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि परमारों के सम्बन्ध में यह संभावना और भी बढ़ जाती है जब हमें ज्ञात होता है कि परमारों का गोत्र ‘वशिष्ठ गोत्र’ है। इसलिए यह बहुत सम्भव है कि परमार मूलतः वशिष्ठ ब्राह्मण थे किंतु बाद में क्षत्रिय माने जाने लगे। संभवतः क्षात्रधर्म अपनाने के कारण अथवा उस वंश के मूल पुरुष ने किसी क्षत्रिय वर्ण की स्त्री से विवाह किया, इस कारण उनके वंशजों ने व्यवहार में अपनी माँ की जाति को अपना लिया जिस प्रकार कि ब्राह्मण हरिश्चन्द्र की क्षत्रिय स्त्री भद्रा की संतान ने स्वयं को क्षत्रिय माना।
दशरथ शर्मा तथा प्रतिपाल भाटिया दोनों ही विद्वानों की यह धारणा कि परमार मूलतः ब्राह्मण थे और बाद में मातृपक्ष की जाति अथवा क्षात्रधर्म अपना लेने के कारण क्षत्रिय समझे जाने लगे, मूल उल्लेख ‘ब्रह्मक्षत्रकुलीन’ शब्द के आशय से बहुत परे है।
ऐसे अनेक उल्लेख मिलते हैं कि ब्राह्मणों ने क्षात्रधर्म स्वीकार किया परंतु उन्हें कहीं भी ‘ब्रह्मक्षत्र’ नहीं कहा गया है। ब्राह्मण पुरुष और क्षत्रिय स्त्री से उत्पन्न संतान को माता की जाति अपनाने के कारण कहीं भी ब्रह्मक्षत्र नहीं कहा गया है।
परमारों की उत्पत्ति वशिष्ट गौत्र से होने के आधार पर उन्हें ब्राह्मण मानने में कुछ आपत्ति है। वशिष्ट गौत्र परमारों के पुरोहितों का हो सकता है जिसे उन्होंने धारण किया हो अतः इन आधारों पर उन्हें मूल रूप में ब्राह्मण मानना उचित नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए ‘ब्रह्मक्षत्रकुल’ पर अधिक विचार करने की आवश्यकता है।
‘ब्रह्मक्षत्रकुल’ शब्द की विद्वानों ने अनेक प्रकार से व्याख्या की है-
1. ब्रह्मक्षत्रकुल वे हैं जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के गुण विद्यमान हों।
2. ऐसा कुल जो मूल रूप में ब्राह्मण हो पर बाद में जिसने क्षात्रधर्म अपना लिया हो, या फिर क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए हों।
3. ऐसा कुल जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही उत्पन्न हुए हों।
4. ऐसा वंश जिसकी उत्पत्ति ब्राह्मण तथा क्षत्रिय स्त्री-पुरुषों के मेल से हुई हो।
इन अर्थों में प्रथम दो अर्थों के लिए साहित्यिक प्रमाण नहीं मिलते। तीसरा अर्थ भी बहुत उचित नहीं कहा जा सकता।
यद्यपि पुराणों में पौरव वंश के अंतिम शासक क्षेमक के बारे में कहा गया है कि ब्रह्मक्षत्र को उत्पन्न करने वाले (ब्रह्मक्षत्रस्य यो योनिर्वशो) तथा देवताओं एवं ऋषियों से सत्कार पाए हुए इस कुल में अंतिम राजा क्षेमक होगा। पौरव क्षत्रिय थे परंतु पौरव राजा अजमीढ़ के वंशजों में काण्वायन [13] और कौशिक [14] ब्राह्मण थे।
चौथा अर्थ सबसे अधिक उपयुक्त है। भारत में राजवंशों में वैवाहिक सम्बन्धों में वर्ण का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता था। अतः एक ब्राह्मण पुरुष और क्षत्रिय कन्या अथवा क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मण कन्या के मध्य विवाह सामान्य रूप से प्रचलित था। इस तरह के विवाहों से उत्पन्न संतानों में दोनों तरह का रक्त विद्यमान होता था। अतः इस तरह की संतानें स्वयं को ब्रह्मक्षत्र कुल का बताना पसंद करती थी। डा. दिनेश चन्द्र सरकार ने इस अर्थ को पुष्ट करने के लिए अनेक अभिलेखों का उल्लेख किया है। [15]
इसी शब्द से मिलता-जुलता शब्द चाटसू और नगर अभिलेखों में ‘ब्रह्मक्षत्रान्वित’ मिलता है। [16] ‘अन्वित’ शब्द का मूल अर्थ सम्बन्धित अथवा जुड़ा हुआ है, अतः इस शब्द का अर्थ होगा- ब्राह्मण और क्षत्रिय से सम्बन्धित, अर्थात् वह एक ही समय में ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही है। इस आशय का अधिक स्पष्टीकरण यह मानने पर हो जाता है कि उसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों का रक्त है। मैसूर के धारवाड़ जिले में चौददनपुर से प्राप्त शक सं. 1139 या ई.1261 से कदम्ब राजा कामदेव के एक ताम्रपत्र से ‘ब्रह्मक्षत्रकुल’ की स्पष्ट व्याख्या होती है। [17]
इस ताम्रपत्र के 10वें श्लोक में कश्मीर राजवंश से सम्बन्धित मायिदेव का उल्लेख हुआ है जो कि साम्प्रायिक सचिव था। मायिदेव के पूर्वजों का उल्लेख करते हुए कहा है कि एक निखकसहा नामक ब्राह्मण कन्या थी, जिसे पाताललोक के नाग राजा ने बहुत समय तक भोगा। इनसे एक नाग वंश की उत्पत्ति हुई और इसी वंश में राजा मुनिजिहर हुआ जो कि मायिदेव का पितामह था। इसमें मायिदेव के माता और पिता का नाम क्रमशः लक्ष्मी और सिगिहर दिया गया है और मायिदेव को ब्रह्मक्षत्र कुल का कहा गया है। [18]
कहने का अभिप्राय यह है कि यह वंश नागवंशी क्षत्रिय राजा एवं ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न हुआ था। उस काल में ‘ब्रह्मक्षत्र’ जैसे शब्द ऐसे लोगों द्वारा प्रयुक्त होते थे जिनमें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों का रक्त विद्यमान था।
इस मत की पुष्टि दक्षिण भारत में मध्यकाल में प्रचलित एक अन्य शब्द से हो सकती है। यह शब्द है ‘ब्रह्मवैश्य।’ वेंगीं के राज्यपाल विक्रमचोड़ (1092-1118 ई.) के शिलालेख में रथकारों को ‘ब्रह्मवैश्यों की सन्तान’ कहा गया है।
धर्मशास्त्रीय नियमों के अनुसार सवर्ण विवाह न करने पर जात्यपकर्ष होता था अर्थात् संतानें अपने पिता के वर्ण से गिर जाती थीं। संभवतः सामाजिक प्रतिष्ठा को अधिक दिखाने के लिए ही उस समय मिश्रित वर्ण की संतानें स्वयं को ब्रह्मक्षत्र अथवा ब्रह्मवैश्य कहने लगीं। अतः ब्रह्मक्षत्र का अभिप्राय यह नहीं है कि कोई कुल ब्राह्मण से क्षत्रिय अथवा क्षत्रिय से ब्राह्मण हुआ बल्कि अपने को ब्रह्मक्षत्र कहने वाला कुल ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही था।
अतः कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति स्वयं को ब्रह्मक्षत्र कुल का कह सकते थे जो कि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय माता-पिता से उत्पन्न हुए हों। परमारों की उत्पत्ति के संदर्भ में भी ब्रह्मक्षत्रकुल शब्द का यही अभिप्राय है कि इनमें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों का रक्त विद्यमान था। परमारों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में और भी कई मत हैं जिनकी चर्चा हम किसी अन्य लेख में करेंगे।
-डॉ. मोहनलाल गुप्ता
सन्दर्भ
[1] राजस्थान भारती, भाग-3, संख्या 2, डा. दशरथ शर्मा का लेख, दी परमार; डा. प्रतिपाल भाटिया, पृ. 7 से 20.
[2] नरेन्द्र प्रकाश जोशी, परमारों की उत्पत्ति विषयक दो प्रमुख धारणाओं की समीक्षा, प्रोसीडिंग्स ऑफ राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस।
[3] (i) एंशिएन्ट मालवा एण्ड दी विक्रमादित्य ट्रेडिशन, पृ. 12; (ii) दी गुहिल्स ऑफ किष्किन्धा, पृ. 19.
[4] नरेन्द्र प्रकाश जोशी, परमारों की उत्पत्ति विषयक दो प्रमुख धारणाओं की समीक्षा, प्रोसीडिंग्स ऑफ राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस।
[5] कादम्बरी, पृष्ठ 17.
[6] कादम्बरी, पृष्ठ 156.
[7] चौखम्बा संस्कृत सीरिज, पृ. 59.
[8] कुवलयमाला कहा, पृ. 50.
[9] एपिग्राफिका इण्डिका, जिल्द 1, भाग 5.
[10] राजस्थान भारती, भाग-3, संख्या 2.
[11] दी परमार, पृष्ठ 19.
[12] ब्रह्मक्षत्रकुलीन प्रलीन सामन्तचक्रनुतचरणः। स्कलसुकृतैकपुंजः श्रीमान्मुंजश्विरं जयति।।
[13] विष्णु पुराण, 4-19.
[14] विष्णु पुराण, 4-7, हरिवंश, 1-27.
[15] दी गुहिल्स ऑफ किष्किन्धा, पृष्ठ 6 से 10.
[16] एपिग्राफिका इण्डिका, खण्ड 12, पृ. 13; भारती कौमुदी, भाग प्रथम, पृ. 267.
[17] जनरल ऑफ दी कर्नाटक यूनिवसिटी, खण्ड 3, संख्या 2, जनवरी 1959, पृ. 57.
[18] एनुअल रिपोर्ट ऑन साउथ इण्डियन एपिग्राफी।