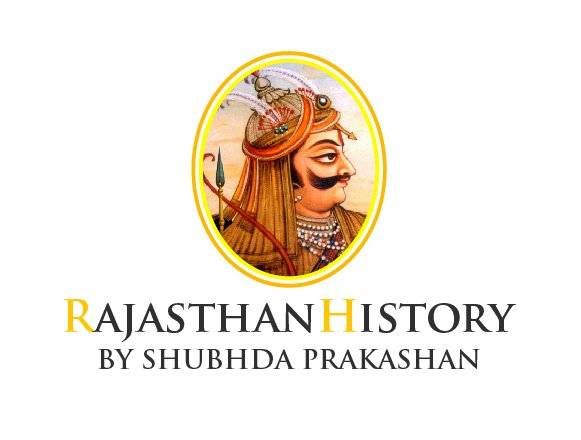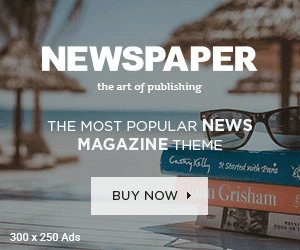मारोठ कुचामन रोड रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित है। यह गांव किसी समय बहुत बड़ा कस्बा था। मूथा नैणसी ने 17वीं शताब्दी में लिखित मारवाड़ रा परगनां री विगत में मारोठ परगना का अलग से विवरण दिया है। इससे स्पष्ट है कि महाराज जसवंतसिंह के शासन काल में मारोठ प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण स्थान था तथा इसे परगना (जिसकी तुलना आधुनिक जिले से की जा सकती है) का दर्जा दिया गया।
कहा जाता है कि मारोठ पहले गराका भैरव के नाम से प्रसिद्ध था। वि.सं. 1010 भाद्रपद सुदि 10 को माठा गुर्जर ने अपने नाम पर यह गांव बसाया।
आरंभ में यह एक छोटी सी बस्ती के रूप में था जो शीघ्र ही इतना फैल गया कि इसके आसपास बसे हुए कई गांव- सोलाण्या, जिनवल, भगवानपुरा, महाराजपुरा, अजीतपुरा, पिरोता का बास, दड़ा का बास, खाती का बास तथा सांगा का बास भी मारोठ में सम्मिलित हो गये। ये सारे गांव मारोठ के लगभग 2 कोस क्षेत्र में फैले हुए थे। अर्थात् तब मारोठ कस्बा लगभग 6 से 7 किलोमीटर की परिधि में फैल गया था।
मारोठ पहाड़ियों के बीच में आया हुआ है, अतः दुर्ग निर्माण की दृष्टि से उपयुक्त है। 11वीं-12वीं शताब्दी से इस पूरे क्षेत्र पर चौहानों के अधीन चन्देल सामंत शासन करते थे। उनकी राजधानी रेवासा में थी। केसरीसिंह चंदेल ने गड़ा के भैरव मंदिर का निर्माण करवाया।
चंदेलों का बनवाया हुआ एक कुआं आज भी गांव में स्थित है जिसे चन्देलों का कुआं कहते हैं। 12वीं सदी में मारोठ चौहान वंशी डाला के अधीन आया। उसके वंशज डालिया कहलाये। उनके नाम पर यह क्षेत्र डालाटी कहलाने लगा। डालिया अधिक समय तक मारोठ को अपने अधीन नहीं रख सके।
किणसरिया (परबतसर से 6 किलोमीटर दूर) अभिलेख में वर्णित दहिया चच्च के छोटे पुत्र विल्हण ने मारोठ पर अधिकार कर लिया। विल्हण ने अपना ठिकाना मारोठ से 6 किलोमीटर दूर देपाड़ा में स्थापित किया। उसके समय का एक छोटा दुर्ग तथा एक सरोवर आज भी देपाड़ा में मौजूद हैं। आज भी कई दहिये अपने आपको देपाड़ा दहिये लिखते हैं। विल्हण एक शक्तिशाली सामंत था। उसे लोकगीतों में स्मरण किया जाता है।
मारवाड़ में आज भी जब दूल्हे की निकासी होती है तो स्त्रियां ‘तेजण है मारोठ री’ मांगलिक गीत गाती हैं। तेजण विल्हण की घोड़ी थी जिस पर बैठकर विल्हण अपने राज्य की देखभाल करता था। दहिये इस क्षेत्र में चौहानों के अधीन सामंतों की स्थिति में थे। जब पृथ्वीराज चौहान (तृतीय) मुहम्मद गौरी से परास्त हो गया तब भी दहिये इस क्षेत्र में बने रहे।
मारोठ के पास मंगलाना से विक्रम संवत् 1272 (ई.1215) का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। इसके अनुसार जिस समय दिल्ली का शासक शम्सुद्दीन गौरी था, उस समय रणथम्भौर के दुर्गपति वल्हणदेव के अधीन दधीच वंशीय महामण्डलेश्वर कदवुराज देव के पौत्र एवं पद्मसिंह के पुत्र महाराज पुत्र जयत्रसिंह देव ने एक बावड़ी बनवाई।
इस शिलालेख से ज्ञात होता है कि उस समय मारोठ के सामन्त महामण्डलेश्वर कहलाते थे। ई.1282 में रणथम्भौर का चौहान हम्मीरदेव दिग्विजय पर निकला तो वह मार्ग के सारे राज्यों को जीतता हुआ मारोठ तक भी आया।
मारोठ क्षेत्र से वि.सं. 1300 का एक शिलालेख मिला है जिसमें दहिया कीर्तिसिंह के पुत्र विक्रम का उल्लेख है। चौदहवीं शताब्दी ईस्वी में नयचन्द्र सूरि ने अपनी पुस्तक ‘हम्मीर महाकाव्य’ में मारोठ को ‘महाराष्ट्र नगर’ लिखा है। मारोठ का यह संस्कृतनिष्ठ नाम 18वीं शती तक की पुस्तकों और लेखों में मिलता है। अपभ्रंश में इसे महारोठ लिखा गया है।
14वीं शताब्दी में गौड़ों ने यह क्षेत्र दहियों से छीन लिया। प्रारम्भिक गौड़ शासकों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। कहा जाता है कि चौहान पृथ्वीराज (तृतीय) के शासन काल में गौड़ बाहर से राजपूताना में आये। आगे चलकर उन्होंने दहियों से मारोठ छीन लिया तथा मारोठ और राजगढ़ (अजमेर के पास) पर शासन करने लगे।
17वीं शताब्दी ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में मारोठ के शासक गोपालदास को आसेरा का किलेदार बनाया गया। गोपालदास तथा उसका पुत्र विक्रम खुर्रम (बाद में शाहजहाँ) द्वारा जहांगीर के विरुद्ध किये गये विद्रोह के समय खुर्रम की तरफ से लड़ते हुए थड़ा की लड़ाई में मारे गए। गोपालदास के बाद उसका पुत्र विट्ठलदास मारोठ का स्वामी हुआ।
गौड़ राजपूतों में विट्ठलदास सबसे अधिक शक्तिशाली था। जब खुर्रम शाहजहाँ के नाम से दिल्ली के तख्त पर बैठा तो उसने विट्ठलदास को ई.1630 में रणथम्भौर का हाकिम नियुक्त किया। ई.1640 में जब वजीर खाँ की मृत्यु हुई तो शाहजहाँ ने विट्ठलदास को आगरा का सूबेदार और किलेदार नियुक्त किया।
ई.1639 में विट्ठलदास के निकट सम्बन्धी बिहारीदास ने मारोठ से राजस्व एकत्र करने वाले चौधरियों से कहा कि वे युद्ध में उजड़े परगनों को फिर से बसायें। उसने चौधरियों को आश्वस्त किया कि जैसी वे सेवा करेंगे वैसा पुरस्कार भी पायेंगे।
विट्ठलदास के बाद उसका पुत्र अर्जुन मारोठ की गद्दी पर बैठा। उसने आम्बेर के कच्छवाहों से मालपुरा (अब जयपुर जिले में) ले लिया। वि.सं.1710 के एक जैन अभिलेख के अनुसार अर्जुन गौड़ के शासनकाल में लालचन्द ने भट्टारक चन्द्रकीर्ति से मूर्तियों की स्थापना का विशाल समारोह आयोजित करवाया।
गौड़ शासक भवन बनवाने के शौकीन थे। उनके बनाये हुए कुछ भवनों के अवशेष आज भी मारोठ में देखे जा सकते हैं। पहाड़ी पर 14वीं शताब्दी में निर्मित लक्ष्मीनारायण मंदिर गौड़ राजपूतों का बनवाया हुआ है। इस मंदिर का अनेक बार जीर्णोद्धार हुआ किंतु अब इस मंदिर का काफी हिस्सा नष्ट हो चुका है।
मारोठ का शिव मंदिर भी गौड़ राजपूतों द्वारा निर्मित है। मारोठ का नौलखा बाग भी गौड़ राजपूतों ने लगवाया। मारोठ के गौड़ राजपूतों से खण्डेला (शेखावाटी) के शेखावतों से शत्रुता चलती रहती थी। मारोठ से 24 किलोमीटर दूर स्थित घाटवा के मैदान में शेखावतों तथा गौड़ों के बीच घमासान हुआ। यह लड़ाई ई.1658 में हुई होगी। इस युद्ध के बारे में एक दोहा कहा जाता है-
गौड़ बुलाव घाटव, चढ़ ओर शेखा
थारी फौजा मारनी, मन देखन का अभिलेखा।
इस युद्ध में शेखावतों को बादशाह औरंगजेब की मूक सहमति प्राप्त थी। गौड़ यह युद्ध हार गये किंतु मारोठ गौड़ों के अधीन बना रहा। ई.1659 में औरंगजेब ने मारोठ परगना अजमेर सूबे में सम्मिलित करके मेड़तिया राजपूत रघुनाथसिंह को दे दिया। गौड़ों ने रघुनाथसिंह को मारोठ सौंपने से मना कर दिया। अतः रघुनाथसिंह ने औरंगजेब से अनुमति प्राप्त करके मारोठ पर चढ़ाई कर दी।
रघुनाथसिंह के साथ उसके ननिहाल एवं ससुराल के शेखावत सरदार भी थे। रघुनाथसिंह की विशाल सेना ने मंगलाणा तथा गांगवा से रोहड़ी तक गौड़ों से संघर्ष किया। मारोठ में गौड़ों से भयंकर युद्ध हुआ जिसमें अनेक गौड़ सरदार मारे गये और कुछ रणभूमि छोड़कर चले गए।
रघुनाथसिंह ने हाथी पर सवार होकर गौड़ों का संहार किया। बचे हुए गौड़ों ने मारोठ गढ़ के दरवाजे भीतर से बन्द कर लिये। मेड़तिया एवं शेखावत सरदारों ने दरवाजा तोड़कर गढ़ में प्रवेश किया। गौड़ राजपूत वहाँ से भाग गये और आस-पास के गांव उजाड़ने लगे।
यह देखकर मेड़तियों ने गौड़ों से अपना वतन न छोड़ने का अनुरोध किया। अतः 17 गांवों में गौड़ बने रहे। रघुनाथसिंह का मनसब बढ़ते-बढ़ते 1500 जात 900 सवार अस्पा हो गई। उसकी नियुक्ति नीमच थाने में की गई जहाँ ई.1680 में उसकी मृत्यु हो गई।
जब रघुनाथसिंह मारोठ का स्वामी हुआ तो उसने राजस्व एकत्र करने वाले चौधरियों के अधिकारों को समाप्त कर दिया। जब चौधरियों ने रघुनाथसिंह का विरोध किया तो रघुनाथसिंह ने कुछ चौधरियों को बन्दी बना लिया।
इस पर भूपत तथा लालचन्द ने जो कि मारोठ के रहने वाले थे, अजमेर के सबूदार के यहाँ दरख्वास्त दी कि रघुनाथसिंह ने श्यामलदास तथा बेलकर्ण को गिरफ्तार कर लिया है, ये दोनों चौधरी कानूनगो की सेवा में थे। ई.1662 में सूबेदार ने श्यामलदास बेलकर्ण की जमानत स्वीकार करके रघुनाथसिंह को आदेश दिया कि श्यामलदास और बेलकर्ण को छोड़ दिया जाये।
सूबेदार ने यह व्यवस्था की कि दो चौधरियों और दो कानूनगो को अपने पद पर बने रहने दिया जाये। इसके बाद श्यामलदास तथा रतनसी को चौधरी के पद पर तथा जसवंत और जेठमल को कानूनगो के पद पर नियुक्त किया गया।
जागीरदारों के गुमाश्तों को निर्देशित किया गया कि वे जागीर के सारे दस्तावेज चौधरी तथा कानूनगो के कहने के अनुसार तैयार करें तथा अजमेर के शाही दफ्तरखाना में जमा करवायें। बिहारीदास ने भी सूबेदार के यहाँ मुकदमा किया कि उसे भी चौधरी बनाया जाये। सूबेदार ने बिहारीदास को भी मारोठ परगने का चौधरी नियुक्त कर दिया।
रघुनाथसिंह के कई पुत्र थे। इनके नाम सबलसिंह, इन्द्रसिंह, विजयसिंह तथा लालसिंह आदि थे। इन सभी ने अपने लिये अलग-अलग गढ़ तथा महल बनाये जिनमें से कुछ आज भी अस्तित्व में हैं। उसके बड़े पुत्र सबलसिंह ने सांवलदास की सेवाओं से प्रसन्न होकर सांवलदास को एक कुंआ तथा 10 बीघा जमीन प्रदान की।
रघुनाथसिंह की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में स्वामित्व को लेकर झगड़ा हुआ। उनकी कमजोरी का लाभ उठाकर जोधपुर नरेश अजीतसिंह ने ई.1708 में मारोठ को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। उसने मायाराम को मारोठ पर अधिकार स्थापित करने भेजा।
अजीतसिंह ने मायाराम से कहा कि इस क्षेत्र के चौधरियों और कानूनगो को वही अधिकार और सुविधाएं दी जायें, जो उन्हें मिलती रही हैं। मारोठ के लिए विशेष फौज नियुक्त की गई तथा उसका व्यय पड़ौसी जागीरदारों से वसूला गया।
11वीं और 12वीं शताब्दी में मारोठ में जैनों का बड़ा प्रभाव रहा। उस काल की अनेक जैन मूर्तियां यहाँ से मिली हैं। इन मूर्तियों के लेखों से ज्ञात होता है कि इनमें से कुछ मूर्तियों की स्थापना 1175 में माथुर संघ के सकलकीर्ति द्वारा करवाई गई थी। मघ्यकालीन चार जैनमंदिर भी मारोठ में मौजूद हैं। ई.1326 में बेनीराम अजमेरा ने आदिनाथ चैत्यालय की स्थापना करवाई। ई.1425 में जीवनदास पाटोदी ने चन्द्रप्रभु चैत्यालय की स्थापना करवाई।
ई.1737 में वैरिशाल के प्रधान अमात्य रामसिंह ने अजमेर के भट्टारक अनन्त कीर्ति से मूर्ति की स्थापना करवाई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रावक एकत्र हुए। ई.1759 में पारसराम ने तेरापंथी मंदिर बनवाया। आदिनाथ चैत्यालय तथा चन्द्रप्रभु चैत्यालय की अनेक बार मरम्मत करवाई गई।
आज भी इन चैत्यालयों का कुछ मूल भाग अस्तित्व में है। आदिनाथ मंदिर के स्तंभ तथा चन्द्रप्रभु मंदिर की छतें कलात्मक ढंग से बनी हैं। मारोठ में कुछ मध्यकालीन छतरियां एवं चबूतरे भी देखे जा सकते हैं।
-इस ब्लॉग में प्रयुक्त सामग्री डॉ. मोहनलाल गुप्ता द्वारा लिखित ग्रंथ नागौर जिले का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास से ली गई है।