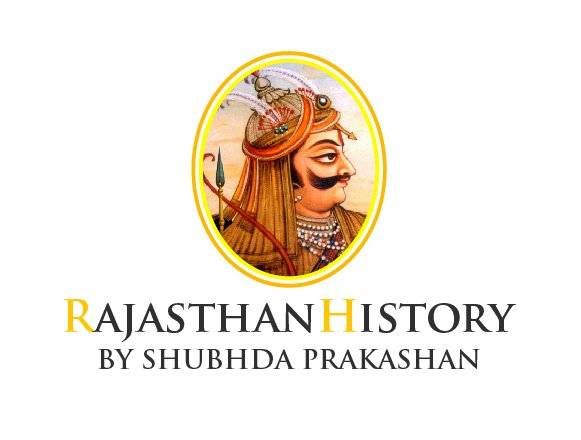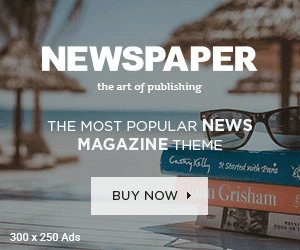राजस्थान में बहीभाट परम्परा सामंती युग की देन थी जो सामंती युग के समापन के साथ ही समाप्त हो गई। एक समय था जब बहीभाट का होना किसी भी राजपूत परिवार के लिए जीवन-मरण के प्रश्न जैसा था किंतु आधुनिक इतिहास लेखन में बहीभाट परम्परा को अधिक आदर नहीं दिया गया।
भारत के प्राचीन आर्य शासकों ने वैदिक काल में जिस वर्णव्यवस्था का सूत्रपात किया, उस वर्णव्यवस्था में शासन करने वाले राजन्य के वंश की उच्चता का गायन करने, उनकी विरुदावलियों का बखान करने तथा राजाओं के वंश की वंशावलियाँ रखने आदि कार्यों के लिए बंदीजन, चारण एवं भाट आदि की परम्पराएं आरम्भ हुईं।
जो मनुष्य राजा के गुणों की वंदना करते थे, उन्हें बंदीजन कहा जाता था, जो मनुष्य चरणों में बंधी अर्थात् कविता के रूप में ढली हुई प्रशस्तियाँ गाते थे, उन्हें चारण कहा गया और जो मनुष्य राजा की भट्टत्व अर्थात् शौर्य का बखान करते हुए गीत गाते थे, उन्हें भाट कहा गया। प्रत्येक आर्य-जन अर्थात् कुल के अपने-अपने बंदीजन, चारण एवं भाट होते थे।
इन कार्यों के बदले में बंदीजनों, चारणों एवं भाटों आदि को राजा के द्वारा पुरस्कार एवं दान-दक्षिणा आदि दी जाती थी। भाटों की परम्परा कब से आरम्भ हुई, इसका कोई इतिहास उपलब्ध नहीं है। रामधारीसिंह दिनकर ने लिखा है कि वर्ण-व्यवस्था आर्यों के भारत आगमन के पूर्व भी प्रचलित थी।[1]
अतः आर्यों के भारत आगमन के समय भाट तथा बन्दीजन उनके कुलों में विद्यमान थे। भाट का सबसे प्राचीनतम उल्लेख ऋग्देव में मिलता है।[2] बहुत से लोक महाभारत के संजय को भाट के अस्तित्व का प्रमाण मानते हैं।
मगध के सम्राट बिम्बिसार के अनेक सजातीय विवाहों का उल्लेख एक आदर्श शासक के रूप में मिलता है। [3] कुछ विद्वान इस विवरण को भाट द्वारा लिखित मानते हैं। कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र में राजा का कुलवान् अर्थात् ‘कुल वाला’ होना आवश्यक बताया है। [4] समकालीन साहित्य में इस परम्परा का निर्वाह न होने पर शासक को कुलहीन की संज्ञा देकर उसे हेय प्रर्दाशत किया गया है। [5]
गुप्तकाल के अभिलेखों पर गुप्त सम्राटों की अनुपम उपलब्धियों के विवरण के साथ साथ उनकी वंशावलियों पर भी अधिक जोर दिया गया है। [6] इससे स्पष्ट है कि वंशावलियां लिखने वाले भाटों का गुप्तकाल के सामान्य जन-जीवन में भी विशेष महत्व रहा होगा।
सामंती युग में बहीभाट के कार्य
राजपूत युग में उनकी जातीय श्रेष्ठता की भावना तथा परस्पर भीषण संघषों के कारण भाटों के पद एवं कार्य दोनों में वृद्धि हुई। [7] उज्जवल वंशावलियों के व्याख्याता बहीभाटों का होना राजपूत सामंती जीवन में अपरिहार्य हो गया- ‘कुल सूनो बिन भाट’ की कहावत इसी युग की देन है। भाट राजपूत सामंती जीवन की अलिखित परम्पराओं का व्याख्याता था जिसके कारण उसे राजपूत समाज में विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ। भाट के प्रमुख कार्य निम्नलिखित थे-
बहीभाट द्वारा इतिहास-संरक्षण
राजपूत काल में राजाओं एवं सामंतों की वंशावलियों को अक्षुण्ण बनाये रखना भाटों का प्रमुख कार्य था। वह प्रत्येक राजपूत-कुल की उत्पत्ति, वंशावली, शाखाओं तथा उपशाखाओं की वंशावलियों का संकलन करता था। वंशावलियों के साथ साथ राजकुल के प्रतापी शासकों द्वारा स्थापित अनेक राजधानियों तथा वहाँ लड़े गये संग्रामों का विवरण भी भाटों की बहियों में मिलता है।
एक ही राजकुल से निकले विभिन्न परिवार अपने बहीभाट को समुचित दान देकर उसकी बही में उल्लिखित अपने पूर्वजों की वंशावलियों में अपने पुत्र-पुत्रियों के जन्म तथा उनके विवाहों के नामों का नामांकन करवाना आवश्यक समझते थे। इस वंश वृक्ष के आधार पर बहीभाट अपने आश्रयदाताओं का ‘कुर्सीनामा’ तैयार रखते थे।
इस प्रकार राजपूत समाज में पैतृक पारिवारिक तथा गोद लेने के उत्तराधिकार सम्बन्धी प्रश्नों में भाट का दिया हुआ निर्णय अन्तिम होता था, जिसे पक्ष तथा विपक्ष के सभी व्यक्तियों को मानना पड़ता था। आज भी भाट के अभाव में राजपूत समाज किसी भी अपरिचित राजपूत को राजपूत मानने में संदेह करता है। राजपूत राज्यों में सामंतों की ‘मातम’ तथा ‘खड्गबन्दी’ करते समय बहीभाटों के ‘कुर्सीनामों’ को देखने की परम्परा प्रचलित थी। [8]
बहीभाट द्वारा आश्रयदाताओं को प्रेरणा
युद्ध के समय भाट तथा चारण कुल के विरुदों, गौरवपूर्ण उपलब्धियों तथा साहसिक कायों पर ओजपूर्ण कविताएं लिखकर अपने आश्रयदाताओं को कुल की परम्परा के अनुरूप श्रेष्ठ एवम् यशस्वी कार्य करने की प्रेरणा देते थे तथा शान्ति के समय वंश की उपलब्धियों का यशोगान करके प्राचीन घटनाओं का स्मरण कराते रहते थे।
अधिकांशतः भाट कवि दानदाता की प्रशंसा में कविता लिखते थे और अन्य कवियों द्वारा की गई कविताओं का संग्रह करके राजसभा में श्रोताओं के समक्ष गाते थे। बहीभाट को राजपूत-कुल की परम्परा और राजा या सामन्त की व्यक्तिगत उपलब्धियों का मूल्यांकन करने का अधिकार भी था।
अतः राजपूत शासक तथा सामन्त भाट को दान-मान देकर प्रसन्न रखने का प्रयास करते थे, अन्यथा बहीभाट गुणगान के स्थान पर दुर्गणों का विश्लेषण कर देता था। [9] ऐसा वर्णन किसी भी यशस्वी एवं स्वाभिमानी राजपूत के लिये अपमानजनक एवं असह्य होता था।
राजपूत कुलों के विवाहों में बहीभाट की भूमिका
राजपूत राजा अथवा सामंत की वंशावलियों में अपने आश्रयदाता राजपूत-कुल के पुत्र-पुत्रियों अथवा राजाओं के अन्य कुलों में हुए विवाहों का उल्लेख भी किया जाता था। बहीभाट इन्हीं वंशावलियों के अनुरूप विवाहों की परम्परा का निर्वाह करने का आदर्श राजपूत-कुल के समक्ष रखते थे। यदि कोई राजपूत विशेष परिस्थिति में उक्त वैवाहिक परम्परा का निर्वाह नहीं करता था, तो भाट उस विवाह का नाम बही में नहीं लिखता और कुटुम्बजनों को बुलाकर कुटुम्ब निर्णय करवाने के उपरान्त ही उसका उल्लेख वंशावली में करता था। [10]
अपने आश्रयदाताओं की खांप तथा कुल के सम्बन्ध में राजपूत समाज में संदेह होने पर बहीभाट ही उसका निराकरण करता था। सम्पूर्ण प्रदेश में राजपूत समाज में परिभ्रमण कर जीविकोपार्जन करने के कारण वह अनेक राजपूत परिवारों के सपर्क में आता था जिसके कारण पुत्र तथा पुत्रियों के उपयुक्त परिवारों में विवाह कराने में भी बहीभाट का सहयोग वांछनीय समझा जाता था। विवाह के प्रश्न पर सहगोत्र के सम्बन्ध में उसका निर्णय अन्तिम होता था। इस मत के समर्थन में एक उदाहरण दिया जाता है-
एक बार किसी अज्ञात कारण से बहीभाटों द्वारा ‘सिरमोर नाहन’ रियासत के राजवंश की संतानों को उपेक्षित कर दिया गया। इस कारण आगे चलकर सिरमोर वंश परिवारों के वैवाहिक सम्बन्ध राजस्थान के राजपूतों में होने में कठिनाई उत्पन्न होने लगी। ‘सिरमोर नाहन’ का राजकुल भाटी वंश से निकला था।
इस कारण उन्होंने भाटियों के बहीभाटों से सम्पर्क स्थापित किया, किन्तु उन्होंने जैसलमेर महारावल की आज्ञा के बिना जैसलमेर एवम् सिरमोर का प्राचीन इतिहास देने से मना कर दिया। इस पर सिरमोर नाहन के राजा ने जैसलमेर के महारावल जवाहरसिंह से ईस्वी 1944 में भेंट कर जैसलमेर के बही भाटों को वहाँ के प्राचीन इतिहास के साथ सिरमोर भिजवाने का अनुरोध किया।
महारावल जवाहरसिंह ने महाराजा सिरमोर नाहन के समक्ष भाटों को वहाँ के प्राचीन इतिहास के साथ सिरमोर भेजना स्वीकार कर लिया और बहीभाट मूलजी के लड़के कल्याणसिंह को उसके डेरे गांव हमीरा से जैसलमेर बुलवाकर जैसलमेर और सिरमोर के सम्बन्धों का ज्ञान महाराजा को कराया।
महाराजा सिरमोर बहीभाट कल्याणसिंह के ऐतिहासिक ज्ञान एवम् स्मरण शक्ति से अत्यधिक प्रभावित हुए और उसे सिरमोर आने का निमन्त्रण दिया। तत्पश्चात् महारावल ने न जाने क्यों, बहीभाट कल्याणसिंह को सिरमोर नहीं जाने का आदेश दिया।
महारावल के आदेशानुसार बहीभाटों के सिरमोर न जाने पर सिरमोर के महाराजा ने बहीभाट मूलजी कल्याणसिंह को सिरमोर बुलाने के लिये अनेक पत्र दिये और अन्त में सिरमोर के दीवान को भी उसके गांव भेजकर उसे साथ लाने का प्रयास किया किंतु दीवान को भी अपने प्रयास में सफलता नहीं मिली।। [11]
बहीभाट द्वारा राजदूत का कार्य करना
मध्यकाल के राजपूत शासक विद्वान बहीभाटों को अपने राजदूत के रूप में अन्य राज्यों में नियुक्त करते थे। बहीभाट की निष्ठा, कार्य कुशलता, सच्चाई तथा योग्यता पर विशेष विश्वास किया जाता था। बहीभाट सदैव आश्रयदाताओं के हितों का परम रक्षक होता था तथा भाट होने के कारण समस्त राजपूत राज्यों में उसे दूत के रूप में श्रद्धापूर्वक देखा जाता था। भाटों ने अनेक राजपूत कुलों एवम् राज्य में होने वाले अनावश्यक पुश्तैनी युद्धों को रोका तथा कलह को शांत करके मित्रवत् सम्बन्ध स्थापित करवाने में प्रशंसनीय भूमिका का निर्वहन किया।[12]
बहीभाट द्वारा त्राग (तागा धार्मिक आत्महत्या)
राजस्थान के सामंती परिवेश में भाट का स्थान विशिष्ट था। उसका न्यायोचित निर्देश नहीं मानना, अपमान करना, कर लगाना, लूटना तथा दान नहीं देना गौ-हत्या के समान पाप माना जाता था। यदि किसी ने ऐसा कर दिया तो समस्त राजपूत कुल ‘कुल की कावड़’ रखने वाले भाट के पक्ष में हो जाते थे और दोषी व्यक्ति से प्रतिशोध लेने का प्रयत्न करते थे। अतः दोषी व्यक्ति के पास भाट से क्षमायाचना करने तथा उसकी क्षतिपूति करने के अतिरिक्त और कोई उपाय शेष नहीं रह जाता था।
किसी राजपूत व्यक्ति द्वारा किसी भाट के साथ कोई घोर अनैतिक व्यवहार किए जाने पर भाट दो-तीन दिन तक भोजन नहीं करता था और अनैतिक कर्म करने वाले राजपूत के विरुद्ध ‘धरणा’ देता था ताकि दोषी राजपूत स्वयं आत्मनिरीक्षण करके अपनी भूल सुधार सके अथवा अन्य व्यक्ति से मध्यस्थता करवाकर भाट की समस्या का समाधान कर सके।
भूल में सुधार न होने पर और भाट के प्रति यथावत अवांछनीय दृष्टिकोण रखने पर भाट स्वयं त्राग [13] (धार्मिक आात्महत्या) करके दोषी के मस्तिष्क पर भंयकर अभिशाप थोपता हुआ उसे समस्त प्रदेश में कुख्यात कर देता था। भाट के वंशज कभी भी उस राजपूत सामन्त के कुल तथा परिवार में याचना करने नहीं जाते थे।
उस राजपूत के वंशज समाज में भाटहीन हो जाते थे तथा दीर्घकाल तक उक्त अशोभनीय घटना पर पश्चाताप एवम् हीनता का अनुभव करते रहते। भाट के आशीर्वाद को शुम एवम् अभिशाप को अशुभ माना जाता था। [14]
बहीभाटों का वर्गीकरण
सामान्यतः राजपूत कुल के बंदीजनों को दो जातियों में विभाजित किया जा सकता है- चारण एवम् बहीभाट। साधारणतः चारणों एवम् भाटों में कोई विशेष अन्तर नहीं होता था। व्यवसायिक दृष्टिकोण से दानों जातियों को राजपूत सामंती जीवन में विशिष्ट स्थान प्राप्त था। दोनों ही जातियां अपने अपने आश्रयदाताओं के उत्साह, देशभक्ति, स्वामिभक्ति, राजभक्ति आथित्य-सत्कार, सरलता, वीरता एवम् दातारी आदि गुणों का यशोगायन करते और बदले में राजपूतों से दान तथा सम्मान प्राप्त करते थे।
भाट मूलतः कुल का लिखित इतिहास वंशावली के रूप में रखता था और आवश्यकता पड़ने पर आश्रयदाताओं को विरुदों के अनुरूप विड़दाता था जबकि चारण अपने आश्रयदाताओं के लिये वीर व्ंयग्यात्मक कविताएं बनाकर कुल-परम्परा के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देता था। यद्यपि राजस्थान में कई विद्वान चारणों ने भाटों की वंशावलियों के आधार पर अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रन्थों का निर्माण किया तथापि उन्होंने वीर-काव्य के प्रणेता के रूप में ही समाज में विशेष ख्याति अर्जित की।
राजपूत परिवारों द्वारा अपनी पुत्र-पुत्रियों तथा विवाह-सम्बन्धों के नामों को बहीभाट की बही में लिखवाने हेतु दान देना पड़ता था जबकि चारणों को वीर काव्य के निर्माण करने पर ही लाखपसाव तथा राजकवि का पद दिया जाता था। प्रत्येक चारण को ऐसा सम्मान मिलना कठिन था। अतः उनमें से अधिकांश को वार्षिक सीख, बधाई तथा विवाहों के अवसर पर वितरित होने वाला ‘त्याग’ लेकर ही जीवन यापन करना पड़ता था। इनका मान तथा सम्मान अधिकांशतः कविता करने पर ही निर्भर था जबकि भाटों के लिये कविता करना आवश्यक नहीं था। [15]
सामंती परिवेश में चारण एवम् भाट दोनों ही राजपूत जाति के समक्ष, ब्राह्मण की भांति आशीर्वाद देने वाले पूज्य व्यक्ति समझे जाते थे। रहन-सहन, रीति-रिवाज एवम् आश्रयदातायों की ओर से जागीरी मिली हुई होने के कारण राजपूत सामंतों की ही भांति इन लोगों को भी राजपूत युग के समाज में उच्च स्थान प्राप्त था।
भाटों का महत्व
राजस्थान के राजपूत कुलों के बहीभाटों का उल्लेख अधिकांश ख्यातों में मिलता है। जैसलमेर के महारावलों ने राज्य में अक्षम्य अपराध करने वाले अपराधियों को बहीभाटों से बहिष्कृत करवाया था। भाटी जसहड़ आसकरण ने जैसलमेर के राज्य सिंहासन को प्राप्त करने हेतु जब महारावल धड़सिह की हत्या भट्टिक संवत 738 (ईस्वी 1351) में की तो मृतक महारावल की रानी विमला देवी तथा अन्य भाटी सामन्तों ने परामर्श करके असहड़ शाखा के भाटियों के नामों को भाट की बही से निकलवा दिया तथा उन्हें भाटी कुल से सदैव के लिये बहिष्कृत करने का प्रयत्न किया।[16]
चूंकि भाट होना राजपूत कुल में अत्यन्त आवश्यक था इसलिये जसहड़ शाखा के भाटियों ने बहीभाट के अभाव में वंशावली तथा अपनी शाखा के सभी नामों को लिखवा कर एक अन्य भाट का आश्रय लिया जिसका भाटी राजवंश के परम्परागत भाटों से कोई सम्बन्ध नहीं है।
वि.सं.1908 (ई.1851) में अंग्रेज सरकार ने जैसलमेर राज्य एवम् जोधपुर राज्य के मध्य पोकरण के समीप सीमांकन का कार्य प्रारम्भ किया। बरडाणे के सामन्त सगतसिंहोत भाटियों ने जैसलमेर महारावल से भाई-बंटवारे में प्राप्त जैसलमेर क्षेत्र के गाँव बरडाणे तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्र का जोधपुर राज्य की सीमा में सीमांकन करवा दिया। जैसलमेर के सीमादल ने इस कार्य का विरोध किया क्योंकि यह गांव तथा उसके आसपास का क्षेत्र मूलतः जैसलमेर राज्य का था।
इस राज्य-घातक अक्षम्य अपराध पर महारावल रणजीतसिंह एवम् अन्य रावलोत, भाटी तथा सोढ़ा सामन्त बरडाणे के भाटियों पर क्षुब्ध हुए किन्तु जैसलमेर राज्य की सीमा में न रह जाने के कारण उन्हें दण्डित नहीं किया जा सका। अतएव महारावल ने बहीभाटों को राजाज्ञा प्राप्त किए बिना बरडाणे के भाटी-सरदारों के यहाँ जाने पर रोक लगा दी। [17]
बहीभाटों के अभाव में बरडाणे के भाटी सगतसिंहोतों ने ‘भाट दूजा करो भले बाप दूजा करो’ की कहावत के अनुसार दूसरा भाट करना पसन्द नहीं किया और लगभग एक शताब्दी तक भाट के अभाव में ही रहे। यद्यपि जसहड़ भाटियों ने दूसरा भाट रख लिया था तथापि बरडाणे के सगतसिंहोत भाटियों ने दूसरा भाट नहीं किया। इस कारण सम्पन्न सामंत होने पर भी, इस काल में उन्हें वैवाहिक सम्बन्धों में कठिनाइयां उत्पन्न होने लगीं और अन्य राजपूत उन्हें संदेह की दृष्टि से देखने लगे।
महारावल रणजीतसिंह (ई.1846-64) से लेकर महारावल जवाहरसिंह (ई.1914-49) तक बरडाणे के सगतसिंहोत भाटियों के प्रति दरबार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मल्लसिंह राजसिंहोत भाटी के नेतृत्व में बरडाणे के सभी सरदारों ने महारावल गिरधरसिंह से इस सम्बन्ध में अनुनय-विनय की। महारावल गिरधरसिंह (ई.1949-51) ने भाटों को बरडाणे के भाटी सगतसिंहोतों के यहाँ जाने और नामों को बही में लिखने का आदेश दिया।
जैसलमेर राज्य के ठिकाना लुहारकी के रावलोत ठाकुर पीरदानसिंह के शासन काल में वि.स. 1980 में उमजी के डेरे के बहीभाट लालजी मूलजी और रावलोत सरदारों में साधारण विषय पर मन-मुटाव हो गया। यद्यपि भाटों ने वहाँ पर ष्तागाष् तो नही किया तथापि वे वहाँ से रुष्ट होकर चले गये।
दीर्घ काल तक लुहारकी ठिकाने में भाटों के नही जाने से उच्चवंशीय रावलोत सरदार प्रदेश एवम् राजपूत समाज मे बहिष्कृत अनुभव करने लगे। लगभग 36 वर्ष बाद में वि.सं.2016 में हीरसिंह के वंशजप्रधान गुलाबसिंह, एस.पी. सुखसिंह दोलतसिंहोत, गिरधरसिंह, मेजर हडुवन्तसिंह (विधानसभा सदस्य), एवम् माधोसिंह ने लालजी भाट के लड़के सांवतजी शैतानजी को समुचित दान देकर पूर्वजों की बही में अपने नाम अंकित करवाकर प्रसन्नता प्रकट की। [18]
बहीभाटों को दान देने की परम्परा
समस्त राजाओं एवं सामंतों द्वारा अपने भाटों को दान दिया जाता था। जैसलमेर के भाटी शासक अपने भाटों को अत्यधिक दान देने में गौरव का अनुभव करते थे।
तवारीख जैसलमेर में देरावर दुर्ग (देवरावर दुर्ग) के निर्माता भाटी रावल देवराज,[19] उतरभिड़किंवाड़ भाटी का विरुद धारण करने वाला रावल लोजा विजयराज, [20] अलाउद्दीन खिलजी के गौरव को आहत करने वाला रावल दूदा [21] तैमूरलंग से युद्ध करने वाला राव केलण, [22] वासणषी के युद्ध का विजेता रावल गजसिंह [23] (ई.1819-45) एवं दानी रावल बैरीसालसिंह [24](1865-91) आदि शासकों द्वारा भाटों को करोड़ों रुपये और कई हाथी तथा ऊंटों को दान में देने का उल्लेख हुआ है।
राजपूत शासकों द्वारा भाटों को दान देने की परम्परा का उल्लेख ने केवल राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों तथा ख्यातों में मिलता है प्रत्युत मध्यकाल की फारसी तवारीख बेगलर नामा भी मिलता है। उसमें सिंध के खान ए जमन ने भाटियों के भाट हेवन्दा को महारावल जैसलमेर के समान सवा करोड़ रुपयों का दान देने का उल्लेख इस प्रकार किया है।
“As the Bhats and Charans were dependents of these chiefs he used to reward these family bards whenever they come to him, with a lakh ( of rupees ?) or more. As Hewanda was the bard of the Bhattis he presented him with a donation of one crore and a quarter, (One hundred and twenty five lakh), besides horses, camels etc. which he like wise generously granted.” [25]
भाटों को दान देने की राजसी परम्परा का अनुकरण प्रदेश के भाटी सामन्त भी करते थे। भैंसड़ा के अमलसिंह जसहड़ ने अपने भाट को लाख पसाव का दान किया था।
[1] रामधारीसिंह दिनकर, संस्कृति के चार अध्याय, पृ. 12.
[2] ऋग्वेद 9, 112, 1-4; एस. एन. दासगुप्ता एण्ड एस. के. डे, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर क्लासीकल पीरियड वोल्यूम फर्स्ट, पृ. 13.
[3] हेमचन्द्र राय चौधरी, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ. 183.
[4] के. पी. जायसवाल, हिन्दू पॉलिटी, अनुवादक रामचन्द्र (हिन्दू राजतंत्र), भाग 2, पृ. 86, 101.
[5] विशाखदत्त, मुद्राराक्षस- अनमिजात कुलहीन।
[6] कुमारगुप्त का करमदण्डा अभिलेख; प्रभावती गुप्त का दानपत्र; स्कन्दगुप्त का भीतरी लेख; भीतरी की राजमुद्रा।
[7] मुहणोत नैणसी की ख्यात भाग-2, काशी संस्करण, अनुवादक रामानारायण दुगड़, पृ. 239, 249, 254, 270, 299, 306,
राजस्थानी भाषा में प्रचलित है-
मात पिता यों बिसरे, बन्धु देय बिसार।
सूरांदाता बातड़ा, चारणभाट चितार।। 1।।
चारण तारण क्षत्रिया, भगता तारण राम।
वे अमरापुर ले चले, ये नवखण्ड राखे नाम।। 2।।
[8] भाटियों के जुवार की बहीभाट की अप्रकाशित ख्यात।
[9] चारण कवि करणीदान ने सवाई जयसिंह जयपुर एवम् अभयसिंह जोधपुर को पुष्कर में खरी खरी सुनाई-
पत जैपुर जोधाणा पत, दोनू ही थाप उथाप।।
कूरम मारियो डिकरो, कमधज मारियो बाप।।
जोधपुर के तख्तसिंह के कार्यों का मूल्यांकन छप्पय में देखिए-
प्रथम तात मारियो, जीवित मात जलाई।
असीच्यार आदमी, हत्या ज्यारी पण आई।
कर गाटो इकलास, वेग जयसिंह बुलायो।
मिट्टी धरण मरजाद, मरम गांठ रो गवांयो।
कवियण हूंत केवा करे, धरा उदक लेवण धरी।
तख्तसी जन्म पायो पछे, किसड़ी बात आछी करी।। 1।।
[10] लखमीचन्द, तवारीख जैसलमेर, पृ. 43; ऊमजी की ख्यात।
[11] स्वर्गीय राव कल्याणसिंह के छोटे भाई अध्यक्ष गजसिंह के साक्षात्कार के अनुसार;प्रो. रतनसिंह, इतिहास के जीवित स्रोत: बहीभाट, राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस प्रोसीडिंग्स, वर्ष 1976.
[12] ऊमजी बहीभाट की अप्रकाशित ख्यात; विद्याधर महाजन, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ. 532; मुहणोत नैणसी की ख्यात भाग-2, काशी संस्करण, अनुवादक रामनारायण दुगड़, पृ. 305.
[13] जेम्स टॉड, राजस्थान का इतिहास, अनुवादक के. के. ठाकुर, पृ. 883.
[14] सूरजमल मिश्रण की बून्दी महाराव को दी गई आशीष (राम रै जाट से उद्धृत)
बधौ तेज धरि विभव, वधौ नति दान बधोतर।
बधौ देश गज बाज, बधोनति राज बीरबर।।
बधौ आर बल बलिन्द, बधौ सुख भोग बधती।
दौलत बधौ दराज, मौज बढ़ो महपती।
……………….. कीटि जुगां राजस करो।। 1।।
[15] सूरजमल मिश्रण ने चारण-भाटों के सम्बन्ध में वीर सतसई में कहा है-
भाट घणां दिन भांखता, कुल भूला भूकन्त।
रहैया नैडे वीर ही, जाण बिरद जवन्त।। 1।।
जो रिण में बिड़दावता, जैं झड़ता खग हुन्त।
वे चारण किण दिश गया, किण दस गा रजपूत।। 2।।
[16] लखमीचन्द, तवारीख जैसलमेर, पृ. 41.
[17] लखमीचन्द, तवारीख जैसलमेर, पृ. 87.
[18] लालजी मूलजी भाट की रावलोतों की बही, प्रधान गुलाबसिंह की प्रशंसा में कहा गया सोरठा एवम् दोहा-
आवे रखकर आस, दीन दुःखी आतुर सभी।
काढ़े सब के काज, दौलत पूत गुलाबसी।। 1।।
गहणों नवगढ माडरो, रावल कुल रो राव।
भाटी जाति चान्दणों, तूँ परधान गुलाब।। 2।।
[19] लखमीचन्द, तवारीख जैसलमेर, पृ. 23.
[20] लखमीचन्द, तवारीख जैसलमेर, पृ. 28.
[21] लखमीचन्द, तवारीख जैसलमेर, पृ. 37.
[22] लखमीचन्द, तवारीख जैसलमेर, पृ.44, राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस प्रोसीडिंग्स, ब्यावर सैशन वर्ष 1973, पृ. 14.
[23] लखमीचन्द, तवारीख जैसलमेर, पृ.79; जगदीशसिंह गहलोत, राजपूताने का इतिहास, भाग 1, पृ. 686.
[24] उपरोक्त, पृ. 95.
[25] इलियट डाउसन, हिस्ट्री ऑफ इण्डिया एज टोल्डन बाई इट्स ओन हिस्टोरियन्स, वोल्यम 1, पृ. 296.