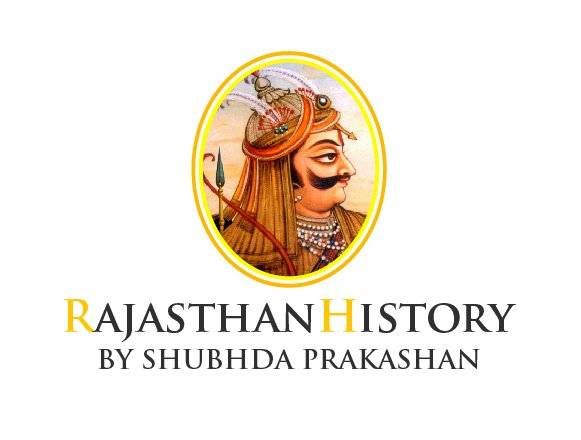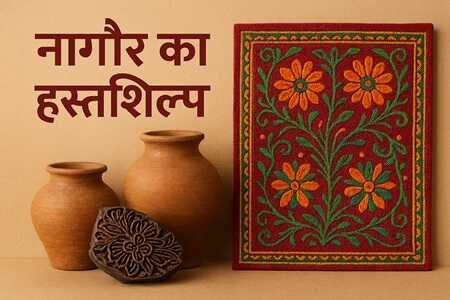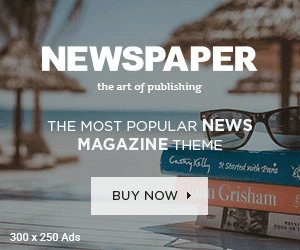नागौर का हस्तशिल्प भारतीय इतिहास की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है। मकराना के संगमरमर ने संसार को आगरा का ताजमहल तथा कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल जैसे भवन दिये तो लोहारपुरा के मुल्तानी लोहारों ने मध्यकालीन इतिहास को भारी भरकम जंगी तोपें बनाकर दीं जिन्होंने भारतीय इतिहास के कई पृष्ठ लिखे।
नागौर का हस्तशिल्प इतनी उत्कृष्ट कोटि का है कि अलौह धातुओं- कांसी तथा पीतल के नागौर में बने कलात्मक बर्तनों की प्रतिस्पर्धा तो कदाचित ही मुरादाबाद या कहीं और के बर्तन कर सकें। किशनगढ़ की बनी-ठनी चित्रशैली को समुद्र पार तक ख्याति दिलवाने वाले कुमावत कलाकार मूलतः नागौर जिले के मारोठ कस्बे की ही देन हैं। चौबीस कैरेट सोने की पत्तियों में इलैक्ट्रोस्टेटिक करंट पैदा करके उनकी जड़ाई के काम में सिद्धहस्त जड़ियों के चालीस परिवार नागौर नगर में रहते हैं।
नागौर, मेड़ता, मारोठ, खाटू तथा डेह आदि कस्बों में पत्थर पर बारीक कारीगरी से बने कलात्मक गवाक्ष भारत भर की स्थापत्य कला से स्पर्धा करने में समर्थ हैं। मारोठ एवं कुचामन का गोल्डन पेंटिंग का काम पूरे देश में विशिष्ट छाप रखता है।
संगमरमर का हस्तशिलप
नागौर जिले अब (डीवाना-कुचामन जिला) के मकराना कस्बे के आसपास की खानों से निकलने वाला संगमरमर पत्थरों का राजा कहलाता है। यह पत्थर श्वेत, मुलायम, चिकना और चमकदार होने के कारण शिल्प जगत में विशिष्ट स्थान रखता है। इस पत्थर से सुन्दर भवनों, मंदिरों, महलों, छतरियों तथा मकबरों से लेकर घर में काम आने वाले खरल, चकले, चौकियां, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल आदि बनते हैं।
मूर्तियों, खिलौनों, सजावटी उपकरणों, जालियों बंदनवारों तथा लघु देवालयों के निर्माण के लिये इसका प्रयोग विशाल स्तर पर किया जाता है। खाटू से प्राप्त पीला पत्थर हस्तशिल्प के लिये जैसलमेर के पीले पत्थर के सदृश्य ही मुलायम, आकर्षक और धारियों से युक्त है। लाडनूं के पास निम्बी जोधा की खानों से गुलाबी पत्थर प्राप्त होता है जिससे कई विशिष्ट कलाकृतियां बनती हैं।
कुंदन का काम
डीडवाना और नागौर में चौबीस कैरेट के सोने की बारीक जड़ाई की जाती है जिसे कुन्दन का काम कहा जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते चले आने के कारण ये परिवार जड़िये कहलाते है। नागौर में इनके चालीस तथा डीडवाना में तीस घर हैं। सोने को पीट-पीट कर उसकी पत्तियों में इलेक्ट्रोस्टेटिक करंट पैदा किया जाता है।
ये छोटी-छोटी पत्तियां विद्युत के प्रभाव से हीरे, पन्ने, एमराल्ड तथा जवाहरात से चिपकाई जाती हैं जिससे आभूषण तथा कालात्मक कृतियाँ बनाई जाती हैं।
गोल्डन पेंटिंग
मारोठ तथा कुचामन में गोल्डन पेंटिंग का काम होता है। मारोठ में इनके आठ तथा कुचामन में चार घर हैं। भारत भर में जितने भी मंदिर है उनमें सोने की कलम का काम कुमावत परिवारों के कारीगरों ने किया है। किशनगढ़ की बनी-ठनी को संसार भर में प्रसिद्ध करने का श्रेय भी कुमावत परिवारों को जाता है।
कुमावत परिवार ड्राई गोल्डन का काम भी करते हैं। मारोठ में गोपाल लाल कुमावत तथा कुचामन में बद्रीप्रसाद और ओमप्रकाश कुमावत इसके सिद्धहस्त कलाकार हैं। कहते हैं मारोठ के कुमावत कारीगर मीठड़ी तथा जावला होते हुए किशनगढ़ पहुंचे।
आज भी किशनगढ़ के गोपाल कुमावत अपनी विशिष्ट चित्रशैली के लिये पूरे भारत में जाने जाते हैं। उन्हें मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित कालिदास पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।
हड्डी, सींग एवं सीप का शिल्प
मेड़ता के कारीगर ऊंट की हड्डियों, गाय-बैल के सींगों तथा सीप आदि साम्री से खिलौने, पशु-पक्षी, कलात्मक डिब्बे, महिलाओं के शृंगार प्रसाधन के डिब्बे, ऐश ट्रे तथा अन्य कलाकृतियाँ बनाते हैं। उन पर रंगों तथा छोटे मनकों की सहायता से आंख, नाक, कान तथा अन्य आकृतियाँ बनाई जाती हैं। ऊंट की हड्डियां अपेक्षाकृत मुलायम होती है तथा इनमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होने से ये अधिक सफेद दिखती हैं।
कलात्मक खाट एवं दरियां
कुचामन, आसपुरा तथा राणसर आदि में खाटों की विविध प्रकार की कलात्मक खाटें बुनी जाती है जो शादी-विवाह में बेटी को उपहार स्वरूप दी जाती हैं। नागौर जिले के टांकला गांव में बनी दरियां दिल्ली के बाजारों में भेजी जाती है।
लाख की चूड़ियां
कुचामन, कूकनवाली तथा मारोठ में लाख की चूड़ियों का अच्छा काम होता है।
सीमेंट एवं पत्थर का शिल्प
कुचामन में सीमेंट की मूर्तियाँ बनाने वाले लगभग 60 परिवार होते हैं। बड़लावास तथा मारोठ में भी सींमेट की मूर्तियां तथा मंदिरों के गेट बनाने वाले कारीगर रहते हैं। छोटी तथा बड़ी खाटू में पत्थर के मेहराब, जाली तथा झरोखे बनाये जाते हैं।
रंगाई-छपाई एवं बंधेज
नागौर में फागण्या पोमचा, पीला, लाडू का ओढ़ना, मोतीचूर का पीला तथा हरा पीला का ओढ़ना एवं साफा की रंगाई होती है। मांग आनेपर साड़िया भी रंगी जाती है। यहां का बना माल गुजरात, महाराष्ट्र तक जाता है। लाडनूं का साफा, चुनरी और साड़ियां प्रसिद्ध हैं। यहां का बना माल कलकत्ता और आसाम तक जाता है। लाडनूं, जसवंतगढ़, कुचामन, डीडवाना, छोटी बेरी, चौलूंखा तथा छोटी छापरी में बंधेज का काम अच्छा होता है।
अन्य हस्तशिल्प एवं सामग्री
बड़ में बनने वाली कशीदा युक्त जूतियों का एक प्रोजक्ट संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यू एन डी पी के तहत चलाया जा रहा है। जिले में सरकण्डों के छाज, मूढ़े तथा अन्य हस्त शिल्प सामग्री बनती है। साटिका में ऊन की कताई तथा पट्ट बनाने का कार्य बड़े पैमाने पर होता है।
मालपुए एवं नमकीन
नागौर के मालपुए और फीणी मूण्डवा के नमकीन सेब (भुजिया) तथा कुचामन के गोंद के पापड़ प्रसिद्ध हैं।
लाहौरपुरा का हस्तशिल्प
नागौर के लौहारपुरा मौहल्ले में मध्यकाल में मुल्तान से आकर बसे मुस्लिम लौहगरों के वंशज आज भी हस्त औजार बनाने का पुश्तैनी काम करते हैं। ये शिल्पी जंत्री कटर, हथौड़े लाँग नोज, एरन, डाई कटर, मिनी मैचर, प्लास, संडासी, फावड़ा, खुरपी, दांतली, छाजला, तसला, सांकल, मोरख, कड़े, गुलमेख, जलेबी की तवी, तथा अन्य कई प्रकार के औजार, उपकरण एवं बरतन बनाते हैं।
ये औजार बड़े पैमाने पर श्नाइजीरिया, अफ्रीका, यूरोप, अमरीका लन्दन, न्यूयार्क, जर्मनी, फ्रांस, इटली तथा रूस आदि को निर्यात किये जाते हैं।
लुहारपुरा में पीतल तथा कांसे के दड़ी, पासे तथा बोरले भी बनाये जाते हैं। प्रतिदिन 35 से 40 किलोग्राम पीतल तथा कांसे के पासे बनाये जाते हैं जो जालन्धर, दिल्ली बम्बई खाड़ी देशों तथा यूरोप को भेजे जाते हैं। साठ दशक से नागौर में कांटे- बाट बनाने का काम हो रहा है।
वर्तमान में नागौर में कांटा-बाट बनाने की पांच इकाइयां हैं जो 3 किलोग्राम से लेकर 50 किलोग्राम तक भार तौलने वाले कांटे तथा बाट बनाती है। 1988 से भारी भरकम ट्रक-ट्रैक्टर बैलगाड़ी आदि तौलने वाले धर्मकांटों का निर्माण भी होने लगा है।